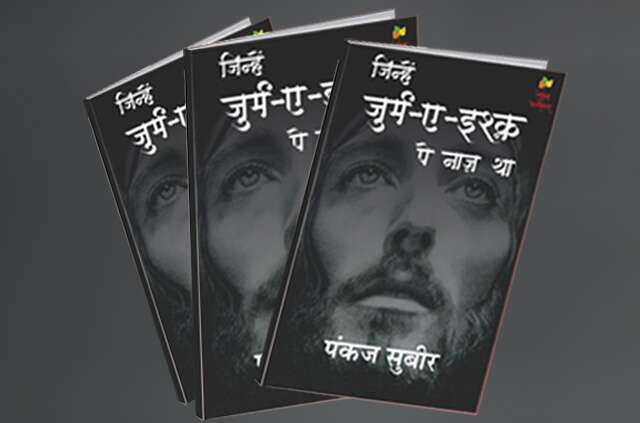गांधीजी- राजनीति और समाजसेवा की परस्परता
वीरेन्द्र जैन
a
गांधी पिछली सदी के महानतम नेताओं में से एक थे। अपने समय के सबसे सशक्त साम्राज्यवाद
के साथ उन्होंने सहज ढंग से उपलब्ध साधनों से ऐसी लड़ाई लड़ी है कि उनके शत्रु भी उनसे
खीझते भले रहे हों पर उनकी निन्दा करने का अवसर नहीं पाते थे। एक अतिसहनशील और परिवर्तनों
के प्रति उदासीन समाज को लड़ाई में साथ लेने की रणनीति तैयार कर लेने में उनका कोई सानी
नहीं था। गांधीजी जब अफ्रीका से लौट कर आये और उन्होंने अपना काम करना प्रारम्भ किया
तो तिलक ने उन्हें सलाह दी कि पहले वे पूरे हिन्दुस्तान को देखें और समझें। सलाह का
पालन करते हुये गांधीजी ने दो वर्ष तक घूम घूम कर गांवों से शहर तक पूरे देश के जनजीवन
को अपनी पूरी गहरी संवेदनशीलता के साथ देखा व बिना किसी पूर्वाग्रह के लोगों के मानस
को पढा। बिहार के चम्पारन जिले में जब एक महिला को उन्होंने नदी तट पर आधी धोती को
धोते ओर सुखाने के बाद शेष आधी धोती को धोते देखा व जाना कि ऐसा करने के पीछे उसके
पास एक ही धोती का होना है तब उनकी समझ में आ गया कि इस देश के लिये उन्हें क्या करना
है।
गांधीजी ने उस दौरान ही समझ लिया था कि बिना सामाजिक परिवर्तन के राजनीतिक लड़ाई
नहीं लड़ी जा सकती। वे विचारों की जड़ता को पसन्द नहीं करते थे और अनुभवों से निकाले
गये निष्कर्षों के आधार पर कभी भी अपने विचार बदल सकते थे। अपने काम के दौरान उन्हें
यह भी समझ में आ गया कि सामाजिक परिवर्तन के लिये समान स्तर पर उतरकर सम्वाद बनाने
की जरूरत होती है व सम्वाद बनाने के लिये न केवल समान भाषा में बातचीत करने की जरूरत
होती है अपितु अपने रहन सहन और पहनावे को सामने वाले के अनुरूप लाये बिना असरकारी सम्वाद
नहीं बनाया जा सकता। जहां नेहरू और जिन्ना का प्रभाव केवल अंग्रेजी ढंग से पढे लिखे
लोगों तक पड़ा वहीं गांधी आम आदमी के पास पहुंचने में सफल हो सके। इंगलैण्ड में पढे
और अफ्रीका में बैरिस्ट्री कर चुके गांधी ने सूट पैंट छोड़ कर धोती लाठी को अपनाया और
खुद की काती हुयी मोटी खादी से बुने हुये कपड़ों को ख़ुशी-खुशी पहना। सबसे महत्वपूर्ण
यह था कि ऐसा उन्होंने तात्कालिक दिखावे या कूटनीति के रूप में नहीं किया, जैसा
कि आज के चुनावी नेता,
चुनाव के समय करते हैं अपितु इसके महत्व को स्वीकारते हुये उन्होंने
इसे दिल से अपना लिया था। जहां नेहरू और जिन्ना के बौद्धिक आतंक और नफासत से आम आदमी
एक दूरी बना कर चलता था वहीं गांधी उसे अपने आदमी लगते थे। गांधी ने न केवल आम आदमी
की भाषा और भूषा का ही स्तेमाल किया अपितु सरल व सस्ते भोजन के लिये उन्होंने शाकाहार
को अपनाया। पर ऐसा नहीं कि वे शाकाहार को सब पर लादते हों। उनके साथ रहने वाले नेहरूजी
प्रति दिन एक अन्डे का सेवन जिन्दगी भर करते रहे और उनके सबसे समर्पित साथी खान अब्दुल
गफ्फार खां जिन्हें खुद सीमांत गांधी के नाम से जाना गया व जो ऐसे अकेले नेता थे जो
विभाजन स्वीकार कर लेने पर गांधीजी के कंधे पर सिर रख कर फूट-फूट रोये थे,जिन्दगी
भर मांसाहारी बने रहे। एक बार बचपन में इंदिरागांधी ने उनसे पूछा था कि क्या मैं अंडा
खा सकती हूं तो बापू ने कहा था कि यदि तुम्हारे घर में खाया जाता है तो तुम खा सकती
हो। गांधीजी ने दूध के लिये भारत के पुराने पौराणिक पशु गाय को नहीं चुना अपितु उन्होंने
सस्ते सुलभ व कम से कम देख भाल की जरूरत वाली बकरी को पाला ,क्योंकि
वह ही गरीब की मां हो सकती थी।
गांधीजी ने लोगों के दिल में इसलिये जगह बनायी क्योंकि वे लोगों के साथ केवल दिमाग
से नहीं जुड़े अपितु दिल और दिमाग दोनों से जुड़े। राजनीति के साथ समाज सेवा करने की आवश्यकता उन्होंने इस कारण महसूस की ताकि लोग
राजनीतिक बात सुनने की स्थिति में तो आयें। वे जानते थे कि कोई भी सम्वाद तभी बनाया
जा सकता है जब सम्बोघित किया जाने वाला व्यक्ति सुनने की स्थिति और तैयारी में हो।
सम्वाद वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता। वे पहले अपने श्रोता की सुनना और उसे समझना ज्यादा
जरूरी समझते थे। ऐसा ही वे अपने तत्कालीन शासकों से चाहते थे। गांधीजी जब माउंटबेटन
से मिलने गये तो वहां कूलर चल रहा था। फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक लपियर कालिन्स के
अनुसार तब सम्भवत: वह भारत में चलने वाला एकमात्र कूलर रहा होगा। गांधीजी बोले- मुझे
सर्दी लग रही है- यह कह कर उन्होंने बातचीत से पहले वहां कूलर बन्द करवा दिया व माउंटबेटन
को बातचीत के मेज पर बराबरी का अहसास करा दिया। वे यह सन्देश देना चाहते थे कि तुम्हारी
मशीनों से चमत्कृत हो मैं अपने यथार्थ को नहीं भूल सकता हूं। उनका एक चम्मच था जिससे
वे दही खाते थे। जब चम्मच टूट गया तब उन्होंने उसमें एक खपच्ची बांध ली थी और लगातार
उसीसे नाशता करते थे। जब लेडी माउंटबेटन ने मेज पर नाश्ता लगवाया तो उन्होंने थैली
में से अपना टूटा चम्मच और दही निकाल लिया। फिर बोले कि मैं अपना नाश्ता अपने साथ लाया
हूं। जिस साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता था उसके प्रतिनिधि के सामने ऐसी विनम्र चुनौती
रखने वाले गांधी सम्वाद में बराबरी का महत्व समझते थे व दूसरों को भी उसका अहसास कराते
रहते थे।
गांधीजी समाज को एक जीवित इकाई की तरह समझते थे और मानते थे कि यदि शरीर की एक
उंगली में दर्द हो तो उसका असर पूरे अंगों पर होता है व उस अंग को ठीक रखे बिना दूसरे
अंगों को ठीक रखना संभव नहीं हो सकता इसलिये वे समाज से केवल गुलामी का ही दर्द नहीं
हटाना चाहते थे अपितु छुआछूत, जातिभेद, गरीबी और रोगों आदि के
साथ समांतर संघर्ष चलाते थे। तत्कालीन समाज में अस्पृश्य मानी जानी वाली जातियों के
साथ बैठकर भोजन करने वाले व अपना पाखाना स्वयं साफ करने की परम्परा डालने वाले गांधी
अछूतोद्धार को भी राजनीतिक लड़ाई से कम महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। वे अपने को आस्तिक
ही नहीं वैष्णव भी बतलाते थे और रोज प्रार्थना
करते थे ,पर यह प्रार्थना सामूहिक होती थी जिसमें सभी धर्मों की प्रार्थनाएं सम्मलित
थीं। उनके एक भजन में अल्लाह ईश्वर एकहि नाम के शब्द आते थे। उनका यह ढंग समाज के सभी
समुदायों को जोड़ने वाला था।
अंग्रेजी साम्राज्यवाद से अहिंसक लड़ाई लड़ने वाला यह योद्धा उपर से ठन्डा दिख सकता
था क्योंकि उसके पास अपने सिद्धांतों और विश्वासों की मजबूती थी। वह इन आन्दोलनों के
दौर में भी कुष्टरोगियों की सेवा भी करता है और अखबार का सम्पादन भी करता है। आज के
पूर्णकालिक राजनेता जो अपने भाषणों में गरीब निर्धन और दलितों के लिये निरंतर घड़ियाली
आंसू बहाते हैं ना तो पर्ल्स पोलियो के दिन बच्चों को पोलियो ड्राप पिलवाने के लिये
निकलते हैं और ना ही सम्पूर्ण साक्षरता आन्दोलन के दौरान लोगों को साक्षरता हेतु अपने
प्रभाव का कोई प्रयास करते नजर आते हैं। यदि राजनेताओं ने गरीबी हटाओं और स्वरोजगार योजनाओं को लागू करवाने को एक राजनीतिक
आन्दोलन की तरह लिया होता तो समाज और उन नेताओं के प्रति विश्वास में जबरदस्त फर्क
आया होता। एक ताजा सर्वेक्षण के अनुसार पचासी प्रतिशत लोग आज के नेताओं की बातों पर
भरोसा नहीं करते हैं। आज राजनीति का अर्थ हो
गया है कि सत्ता में अपने आप को अपनी क्षमताओं से अधिक ऊंचे स्थान पर फिट करने के लिये
प्रयत्नशील रहना व ऐसा होने में अवरोध बनने वालों का विरोध करना। जिस दल के कार्यकर्ता
सत्ता के लाभों के अभ्यस्त हो जाते हैं वे सत्ता चली जाने के बाद लुंजपुंज हो जाते
हैं जबकि लोगों को उनके विधिसम्मत अधिकार दिलवाने के लिये संघर्ष करने का यह सर्वोत्तम
अवसर होता है। भाषणों में देश के लिये खून की एक एक बूंद देने का दावा करने वाले यदि
राष्ट्रीय त्योहारों पर रक्तदान की परंपरा ही डालें तो इस देश के किसी अस्पताल को कभी
रक्त की कमी न पड़े और प्रतिवर्ष हजारों जानें बच सकें। गांधीजी अगर आज होते तो उन्होंने
ऐसा ही कोई ढंग चुना होता। किस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वर्ष में कितना रक्त दान
किया है इसका आंकड़ा न केवल उस पार्टीवालों का देशवासियों के प्रति समर्पण ही प्रकट
करेगा अपितु उनके त्याग की परीक्षा भी करेगा। श्री नरेन्द्र मोदी भी स्वच्छता को
भाजपा का कार्यक्रम नहीं बना सके हैं, जो केवल सरकारी तमाशा बन कर रह गया है।
खेद की बात तो यह है कि जिन लोगों के पास गांधी की विरासत थी वे उसका उपयोग नहीं
कर रहे हैं और गांधीवाद के शत्रु उनकी रणनीतियों का सर्वाधिक कुटिलतापूर्वक स्तेमाल
कर रहे हैं। जब ग्यारह सितम्बर दो हजार दो को वर्ल्ड ट्रेड सैंटर पर आतंकियों ने हमला
किया तो उसमें सबसे अधिक उल्लेखनीय तथ्य यह था कि उन हमलावरों ने अमेरिका के ही विमानों
का अपहरण करके और उनके महत्वपूर्ण स्थलों पर टकराकर धाराशायी कर दिया। मुझे इस घटना
के समय इन अर्थों में गांधीजी की याद आयी कि अगर किसी के पास इरादे हों तो संघर्ष के
लिये बाहरी संसाधनों की जरूरत नहीं होती और अपनी जान को दांव पर लगा देने के आगे सारे
हथियार बेकार होते हैं। गांधीजी इसे अपने अच्छे कार्यों के लिये अच्छे ढंग से प्रयोग
करते थे। चुनाव के समय जनता की सेवा के दावे करने वाले नेता चुनाव हार जाने पर जनता
की सेवा से दूर क्यों हो जाते हैं या केवल छुटपुट विरोध प्रर्दशनों तक अपने को सीमित
क्यों कर लेते हैं?
क्या जनता की सेवा किसी पद के लिये चुने जाकर ही की जा सकती
है?गांधी बिना किसी पद पर रहे कुष्टरोगियों की सेवा करते थे, अछूतोद्धार
करते थे, सूत कातते थे और हिन्दी प्रचार सभा चलवाते थे। आज यदि साम्प्रदायिक संगठन
अपनी जगह बना सके हैं तो उसके पीछे उनका जनसेवा के स्थलों पर दिखना भी है। उनको निर्मूल
करने की इच्छा रखने वालों को गांधी के रास्ते पर चलकर सबसे पहले समाजसेवा में उनसे
आगे निकल कर दिखाना होगा। समाजसेवा के कार्यों को सरकारी मशीनरी के भरोसे नहीं छोड़ा
जा सकता तथा सरकारी मशीनरी के द्वारा वांछित परिणाम पाने के लिये राजनीतिक संगठनों
का सक्रिय हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया है। पर, किसी भी दल की घोषणाओं में सरकार से बाहर
रहते हुये किये जाने वाले सामाजिक कार्यक्रमों की चर्चा तक नहीं की जाती। गांधीजी दहेजप्रथा, सतीप्रथा
आदि कुरीतियों से टकराने को सदैव तत्पर रहते थे पर आज उनके नाम पर राजनीति करने वाले
वोटों के लालच में विभिन्न समाजों की कुप्रथाओं को न केवल संरक्षण देते हैं अपितु कानूनी
दायरे में आने पर उन्हें बचाने का काम भी करते हैं।
गांधीवादी राजनीति का दावा करने वाले दलों के सदस्य यदि प्रतिमाह केवल एक सामाजिक
कार्य में ईमानदारी से सहयोंगी होने का कार्यक्रम बनाकर चलें तो उनकी लोकप्रियता में
गुणात्मक परिवर्तन दिख सकता है। गांधीवाद की सबसे बड़ी विशेषता सिद्धांतों और व्यवहारिकता
को समानान्तर ढंग से चलाना है। गांधीजी ने अपनी जिन्दगी में इसे सफलतापूर्वक करके दिखाया
है।
वीरेन्द्र जैन
2/1 शालीमार
स्टर्लिंग रायसेन रोड
अप्सरा सिनेमा के पास भोपाल [म.प्र.] 462023
मोबाइल 9425674629